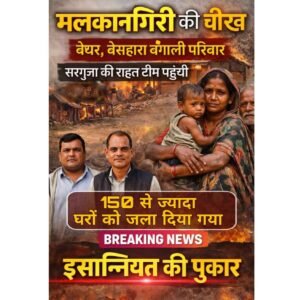झूठा आरोप लगाकर निर्दोष व्यक्ति को फंसाने वाले के खिलाफ किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा, पढ़िए एआईपीसी 211
पत्रकार – महेंद्र सिंह लहरिया
झूठ-झूठ अक्सर ऐसा हम सुनते आ रहे हैं। कोई निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया जाता है और उस पर दाण्डिक कार्यवाही बैठा दी जाती है, और बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है किसी अन्य व्यक्ति ने भेदभाव की भावना को रखते हुए उस पर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की है। आप उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसने आपको झूठे आरोप में दाण्डिक कार्यवाही बैठाई थी। उस पर भी मुकदमा एवं एफआईआर दायर कर सकते हैं।
भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 211 की परिभाषा:-
कोई व्यक्ति किसी निर्दोष व्यक्ति पर उसको नुकसान या क्षति पहुचाने के उद्देश्य से दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करेगा या झूठा आपराधिक आरोप लगाएगा इस धारा के अंतर्गत अपराध है।
नोट:- यह अपराध तब घटित होता है जब झूठे आरोप पुलिस या मजिस्ट्रेट के पास लगाया गया है तथा वहीं से दाण्डिक कार्यवाही की जा रही हो। केवल संदेह करना झूठा आरोप नहीं माना जायेगा एवं झूठी सूचना देना मात्र भी इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 211 में दण्ड का प्रावधान:-
इस धारा के अपराध असंज्ञेय एवं जमानतीय होते है। इनकी सुनवाई प्रथम श्रेणी के
मजिस्ट्रेट ओर सेशन न्यायालय दूआरा की जाती हैं !
सजा :- सजा की निम्न भागों में बांटा गया है:-
- क्षति(नुकसान) करने के आशय से झूठा आरोप लगाने पर- दो वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
- आरोप सात वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय है तब- सात वर्ष की कारावास और जुर्माना से दण्डनीय होगा।
- आरोप मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय हैं तब- सुनवाई सेशन न्यायालय दूआरा एवं सात वर्ष की कारावास एव जुर्माना से दण्डनीय होगा।
नोट:- छत्तीसगढ़ राज्य संशोधन अधिनियम,2013 (प्रभावशाली दिनांक 21/07/2015) के अंतर्गत
4.आरोपित अपराध धारा- 354,354क,354ख,354ग,354घ,354ङ, 376ख,376ग,376च,509,509क, 509ख से दण्डनीय अपराध की सजा- कारावास तीन वर्ष से कम नहीं लेकिन 5 वर्ष तक हो सकती हैं जुर्माने के साथ।
उधारानुसार:- किसी व्यक्ति ने पुलिस को किसी अपराध की झूठी सूचना देते हुए यह आशंका व्यक्त की कोई अन्य व्यक्ति भी इस अपराध में शामिल होने का शक है, अगर यह सूचना झूठी पाई जाने के आधार पर उस सूचना देने वाले व्यक्ति पर धारा 211 के अंतर्गत कार्यवाही नही की जा सकती है। लेकिन जहां उस व्यक्ति की रिपोर्ट से यह उद्देश्य स्पष्ट झलकता है तब उस निर्दोष व्यक्ति को हिरासत में लिये जाने एवं उसके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जाने की अपेक्षा करता है, तब वह सूचना झूठी साबित होने पर उसके विरुद्ध धारा 211 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
*कंपनी समय पर सैलरी ना दे तो क्या करें।*
भारतीय कानून कर्मचारियों/एम्प्लॉईज़ को उनके अधिकारों के लिए बहुत सुरक्षा देता है। काम कराने के लिए एम्प्लॉईज़ को हायर करने वाले नियोक्ता आमतौर पर मानते हैं कि एम्प्लॉईज़, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने अधिकारों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, इसलिए वे उन्हें किसी भी समय कंपनी से टर्मिनेट कर सकते हैं या आसानी से उनकी सैलरी देने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि, कानून एम्प्लॉईज़ की कम सैलरी, उचित कमाई आदि जैसे सभी अधिकारों की रक्षा करता है।
कानून:
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (न्यूनतम वेतन अधिनियम) और मजदूरी अधिनियम का भुगतान (मजदूरी भुगतान अधिनियम) दो और ऐसे क़ानून हैं जो मजदूरी अधिनियम (वेतन अधिनियम) में शामिल हैं। एम्प्लॉईज़ को उनके नियोक्ताओं द्वारा सैलरी कैसे दी जाती है, इसे नियंत्रित करने वाले यह दो प्राथमिक कानून हैं। सभी एम्प्लॉईज़ को न्यूनतम सैलरी का अधिकार है, जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में तय किया गया है। एम्प्लॉईज़ जिस तरह का काम करते है, उस काम के मुताबिक ही कम से कम सैलरी तय की गयी है।
हालाँकि, राज्य-दर-राज्य यह अलग-अलग होती है। वेतन भुगतान अधिनियम (वेतन भुगतान अधिनियम) और अन्य क़ानून, नियोक्ताओं को सैलरी समय से और सही तरीके से मिलने से संबंधित है। सरकार ने इन कानूनों के गलत तरह से अनुपालन होने या पालन ना होने से संबंधित मैटर्स की निगरानी के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को तय की गयी कम से कम सैलरी जरूर मिले। वह ऑफिसर्स हैं:
एम्प्लॉईज़ के मुआवजे/कंपनसेशन के लिए एक कमिशन की नियुक्ति/हायरिंग*
इन संघर्षों की निगरानी के लिए एक रीजनल लेबर कमीशन का इंचार्ज
इस तरह के मैटर्स में, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का प्रीसिडिंग ऑफ़िसर एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है।
सैलरी भुगतान एक्ट का सेक्शन 4, सैलरी देने के बारे में बात करता है और बताता है कि इसे बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं बल्कि केवल एक निश्चित समय के लिए ही बढ़ाया जा सकता है।
जब अलग-अलग राज्यों में मौजूद दुकानों के व्यवहार को विनियमित करने की बात आती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई राज्यों में सैलरी के भुगतान के संबंध में अलग-अलग नियम और कानून होते हैं। इसे “दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम” (दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम) के रूप में जाना जाता है। हालांकि, मॉडल कानून, जो राज्य में बने नियमों को स्थापित करता है, यह भी तय करता है कि अगर एम्प्लोयी सामान्य से ज्यादा समय तक काम करता है तो उसे दोगुना मुआवजा मिलना चाहिए। अगर नियोक्ता इन सिचुऎशन्स में भुगतान करने में विफल रहता है, तो लगभग 2 लाख का जुर्माना लगाया जाता है।
कॉन्ट्रक्ट लेबर एक्ट के सेक्शन 21 में यह आदेश दिया गया है कि कांट्रेक्टर उन एम्प्लॉईज़ को भुगतान करते हैं जिन्हें वे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर हायर करते हैं। अगर ऐसा भुगतान नहीं किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर हायर किये हुए एम्प्लोयी को भुगतान करने के लिए प्राथमिक नियोक्ता जिम्मेदार होता है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम (औद्योगिक विवाद अधिनियम) के सेक्शन 33सी में उस धन की चर्चा है जो एम्प्लोयी पर बकाया है और इसे कैसे प्राप्त किया जाए। जब किसी एम्प्लोयी पर पैसा बकाया होता है, तो वह उपयुक्त कोर्ट में केस फाइल कर सकता है और अगर कोर्ट बताए गए दावों की वैलिडिटी के बारे में आश्वस्त है, तो पैसे की रिकवरी की जा सकती है। यह क्लॉज़ उन सिचुऎशन्स को भी संबोधित करता है, जिनमें एक एम्प्लोयी की मृत्यु हो जाता है और कंपनी को एम्प्लोयी के उत्तराधिकारियों को अवैतनिक सैलरी की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए।
2013 का कंपनी एक्ट के सेक्शन 447 धोखाधड़ी के लिए सज़ा देता है। कम से कम छह महीने और ज़्यादा दस साल की जेल। एक जुर्माना जो धोखाधड़ी की अमाउंट से कम नहीं हो सकता है और धोखाधड़ी की राशि के तीन गुना से कम नहीं हो सकता है।
सैलरी का भुगतान ना होने पर उठाए जाने वाले कदम:
वेरिफिकेशन के रूप में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बैंक की डिटेल्स से संबंधित अटार्नी की जानकारी दें। सैलरी ना देने के परिणामों/रिजल्ट्स का उल्लेख करें और नियोक्ता को नोटिस भेजें।
सैलरी का भुगतान ना होने से संबंधित परेशानी होने पर एम्प्लोयी, लेबर कमीशन से संपर्क कर सकता है। सिचुएशन की जांच करने के बाद वह कोई समाधान/सोल्युशन निकालेंगे। समाधान नहीं होने पर मैटर को कोर्ट में पेश किया जा सकता है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम (औद्योगिक विवाद अधिनियम)के सेक्शन 33सी के तहत एम्प्लोयी केस फाइल कर सकता है, अगर लेबर कमीशन द्वारा मैटर सुलझाने में परेशानियां आ रही है। हालांकि, एम्प्लोयी सैलरी ना मिलने के एक साल के अंदर केस फाइल कर सकता है, और कोर्ट फैसला लेने में तीन महीने से ज्यादा समय नहीं ले सकती है।
ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अब एक आर्बिट्रेशन क्लॉज़ शामिल होता है क्योंकि यह मैटर को सुलझाने का सबसे लोकप्रिय प्रोसेस में से एक है। अगर किसी भी प्रकार का डिफ़ॉल्ट हुआ है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मैटर का फैसला कर सकता है।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दिवाला और दिवालियापन संहिता) की शर्तों के तहत, एनसीएलटी/ एनसीएलटी में भी एक अनुरोध/रिक्वेस्ट की जा सकती है, बशर्ते बकाया सैलरी कम से कम 1 लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी से लाभ प्राप्त किया है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें वापस भुगतान करें। इसे क्वांटम मेरिट और अन्यायपूर्ण संवर्धन (क्वांटम योग्यता और अन्यायपूर्ण संवर्धन) भी कहा जाता है। एम्प्लोयी को सैलरी भुगतान करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है क्योंकि एक संगठन/आर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लोयी की मदद के बिना ग्रो/विकास नहीं कर सकती है।